(08-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

:08-01-22
The 1-in-31 issue
House committees reflect larger male bias
TOI Editorials
Women MPs surely should have a strong say on the proposed Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill that seeks to raise the legal age of marriage for women to 21. But, as has been widely reported, the bill has been referred to a parliamentary standing committee – on education, women, children, youth and sports – that has exactly one woman MP out of 31 members. The fault is not this or that committee’s. The fault lies in how dominant male politicians who decide on committees, and election candidates think.
For example, while at 110 – 81 in Lok Sabha and 29 in Rajya Sabha – the proportion of women in the 779-strong Parliament is still a low 14%, a standing committee on women’s issues doesn’t even reflect this proportion, nowhere close to it. Just one woman member in a 31-strong committee means women have 3% representation in a group that will decide the fate of millions of young women.
Data shows that women candidates have as good an electoral strike rate as their male counterparts. And politically investing in women is not just fair but also common sense with participation of women voters steadily increasing. Female voter turnout in the last Lok Sabha polls outdid male participation by 0.17 percentage points. This is new India. How long will our male netas across parties ignore it?
Date:08-01-22
Why India needs a fiscal council
Budget process is too arbitrary and it needs another layer of scrutiny
M Govinda Rao, [ The writer is former Director, NIPFP and Member, 14th Finance Commission. He is now Chief Economic Adviser, Brickwork Ratings.]
On December 13, 2021, the Union Minister of State for Finance in a written reply to the Parliament ruled out setting up of a fiscal council as recommended by the FRBM Review Committee. The reasoning given for the rejection was that there are institutions such as the Comptroller and Auditor General (CAG), National Statistical Commission and the Finance Commission that already perform some or all of the proposed functions of the Fiscal Council.
But 30 developed and emerging market economies have found it necessary to have such an institution. These are called Congressional Budget Office in the US, Office of Budget Responsibility in the UK, Parliamentary Budget Office in Australia, and Fiscal Council in many other countries.
Listen to the Finance Commission’s argument
The 15th Finance Commission also argued that setting up a Fiscal Council is an essential part of the 21st century fiscal architecture. Case studies by the IMF and OECD confirm that independent fiscal institutions have been effective complements to fiscal rules in monitoring their effective implementation and have contributed to improved fiscal performances.
The 15th Finance Commission had said, “Absence of an independent fiscal institution to assess and evaluate the fiscal plan as well as performance and forecasts published by the governments (as is now the reality in any advanced and emerging market economies) has further diminished the capacity to monitor compliance. ”
Unfortunately, the Explanatory Memorandums containing the Action Taken Report on the 13th, 14th and 15th Finance Commissions placed in Parliament are silent on this recommendation.
The objective of establishing the Fiscal Council is to have an ex-ante evaluation including the robustness of budget forecasts, work out costs of various budget proposals to evaluate the realism of the budget estimates, and monitor progress and conformity to fiscal rules. This is clearly different from ex-post analysis undertaken by the CAG or the Statistical Commission or the Finance Commission.
The 15th Finance Commission has listed a number of functions for the Fiscal Council and these are
Providing multi-year macro-economic and fiscal forecasts,
Evaluating fiscal performances vis-à-vis targets across all levels of government,
Assessing the appropriateness and consistency of fiscal targets in the states,
Undertaking independent assessment of longterm fiscal sustainability,
Assessing fiscal policy statements by governments under fiscal responsibility legislations,
Advising on the conditions for using escape clauses under fiscal responsibility legislations,
Policy costing of new measures with significant fiscal implications,
Providing analytical support to the Finance Commissions, and ? Publishing of all their reports and underlying methodologies.
FRBM mechanism hasn’t delivered
There are no independent institutions to undertake these tasks at present and setting up of the Fiscal Council is intended to enhance the effectiveness of the FRBM process. The experience with the implementation of FRBM so far shows that the performance has been disappointing.
FRBM compliance reports of the CAG, the detailed analysis of the Finance Commissions as well as individual researchers show that the FRBM process as it exists now has several shortcomings in its failure to achieve the fiscal targets and also raise doubts on the credibility of budgets due to shifting goal posts, taking pauses, attributing the slippage to imaginary factors, creative accounting, creating new concepts such as effective revenue deficit, off-budget financing of expenditures, and loan intermediation through public enterprises.
The essential logic for having the Fiscal Council is that when the markets fail governments should intervene and to safeguard against government failure, it is necessary to have systems and institutions put in place and a Fiscal Council is an important institution to ensure efficient calibration of fiscal policy.
The question then is whether a Fiscal Council will ensure the achievement of the objectives assigned to it. The answer is that it is certainly not a ‘silver bullet’. If the government of the day has the political will to contain deficits and debt at sustainable levels, the institution will be superfluous.
On the other hand, if there is no political will, having such an institution will not make much difference. However, like the FRBM process itself, it helps to bring in an additional layer of legislative scrutiny, raise public awareness and makes the system more comprehensive and transparent.

Date:08-01-22
A serious lapse
An improved protocol for the PM’s travel, and a repurposing of the SPG might be necessary
Editorial
The lapse in Prime Minister Narendra Modi’s security arrangements, which left his convoy stranded on a flyover for around 20 minutes, near Ferozepur in Punjab on Wednesday is indeed a serious one as stated by the Union Home Ministry. But by quickly blaming the Punjab government and the State police, the Central functionaries triggered a blame game that has forestalled the possibility of a fair and credible inquiry into the incident. Two parallel inquiries have been announced, one by the Centre and another by the State, both of which are on hold until Monday when the Supreme Court of India will hear a plea on the issue. Discussions on national security are always surcharged in India but at least this one involving the personal security of the Prime Minister should have been more tempered. Union Ministers and Bharatiya Janata Party functionaries turned this into yet another loyalty test, and resorted to hyperbole. India takes the security of its Prime Minister very seriously. After all, a sitting Prime Minister, a former Prime Minister, and the leader revered as the father of the nation are among the list of the country’s assassinated leaders. The Special Protection Group (SPG), with an outlay of around ₹600 crore in 2020 and around 3,000 personnel has just one job — protect one person, the Prime Minister.
The critical question that is to be probed is who made the decision that the Prime Minister could, and should, travel by road for more than 100 km, from Bathinda to Ferozepur and what inputs went into making that decision. Assuming that someone concluded that it was advisable for the Prime Minister to be on the road for nearly two hours, the process that preceded it must be probed. It was also decided that the Prime Minister should not be using a helicopter as was originally planned. The route was identified in advance as a contingency plan, but the decision to use it was made at the last moment — a version that both the State and Central governments agree on. Various scenarios involving miscommunication, misinformation and misjudgment are possible. Protesters who blocked the route were reportedly unaware of the Prime Minister’s travel. As the Union Home Minister said, accountability must be fixed, and loopholes must be plugged. Considering the mutual distrust the State and the Centre have now public, a Supreme Court-monitored probe could be a good way to get to the bottom of the matter in a credible manner. This episode must also lead to a more efficient protocol for the Prime Minister’s travel, and a repurposing of the SPG, if required. Meanwhile, loose talk, diatribe and electioneering on the issue must be shunned at all cost.
Date:08-01-22
The baton of forest restoration in the net zero race
For carbon sequestration, India must revisit its policy framework and reverse fading participation of local communities
Mohan Chandra Pargaien, [ Mohan Chandra Pargaien is Senior IFS officer, Hyderabad, Telangana.]
 India’s pledge to set a net zero target by 2070, at the COP26 summit, Glasgow, has again highlighted the importance of forests as an undisputed mechanism to help mitigate the challenges of climate change. Though, in more specific terms, this was already highlighted during the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) framework (2013) of REDD+ for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, along with the ‘sustainable management of forests for the conservation and enhancement of forest carbon stocks’. In a study by Griscom (2017), land-based sinks (natural climate solutions which also include forests) can provide up to 37% of emission reduction and help in keeping the global temperature below 2° C. Further, recent research has favoured a natural regeneration model of restoration over the existing much-hyped mode of tree planting as such forests are said to secure nearly 32% carbon storage, as per one report of the ntergovernmental Panel on Climate Change.
India’s pledge to set a net zero target by 2070, at the COP26 summit, Glasgow, has again highlighted the importance of forests as an undisputed mechanism to help mitigate the challenges of climate change. Though, in more specific terms, this was already highlighted during the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) framework (2013) of REDD+ for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, along with the ‘sustainable management of forests for the conservation and enhancement of forest carbon stocks’. In a study by Griscom (2017), land-based sinks (natural climate solutions which also include forests) can provide up to 37% of emission reduction and help in keeping the global temperature below 2° C. Further, recent research has favoured a natural regeneration model of restoration over the existing much-hyped mode of tree planting as such forests are said to secure nearly 32% carbon storage, as per one report of the ntergovernmental Panel on Climate Change.
Continued degradation
Though India is said to have increased its forest cover by 15,000 square kilometres in the last six years, the degradation of existing forests continues. As per the State of Forests Report (1989), the country had 2,57,409 sq.km (7.83% of its geographical area) under the open forest category, having a density of 10% to less than 40%. However, in 30 years (2019) this has been increased to 3,04,499 sq.km (9.26%). This means every year on average, nearly 1.57 lakh hectare of forests was degraded. This degradation highlights the presence of anthropogenic pressures including encroachment, grazing, fire, which our forests are subjected to. Having diverted nearly 1.5 million hectares of forests since 1980 for developmental activities and losing nearly 1.48 million hectares of forests to encroachers coupled with an intricate link between poverty and unemployment, India is witnessing enormous degradation of forests and deforestation. This warrants the participation of people as an essential and effective route to achieve the desired target of carbon sequestration through the restoration of forests.
Terms of engagement
In a historic departure from pursuing commercial objectives to supporting the needs of people in a participatory manner (as envisaged in National Forest Policy, 1988), India made its attempt, in 1990, to engage local communities in a partnership mode while protecting and managing forests and restoring wastelands with the concept of care and share. This concept of joint forest management spelt much hope for States and forest-fringe communities. Later, the concept of forest development agencies was introduced to consolidate the efforts in an autonomous model, which paved the way for fund flow from various other sources to joint forest management committees. The efforts to make this participatory approach operative resulted in the formation of nearly 1.18 lakh joint forest management committees managing over 25 million hectares of forest area. Most of these became active and operative while implementing various projects financed by external agencies such as the World Bank, the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Japan, the Department for International Development (DFID) United Kingdom and the European Union (EU). The similar system of joint management in the case of national parks, sanctuaries and tiger reserves which existed in the name of eco-development committees initially proved effective as it could garner the support of these participating communities not only for the protection and development of biodiversity but also in the considerable reduction in man-animal conflicts and the protection of forests from fires and grazing.
However, the completion of the project period and lack of subsequent funding affected their functionality and also the protection of forests due to a lack of support from participating local communities including associated non-governmental organisations.
Except for the National Mission for Green India, in all other centrally sponsored programmes such as Project Tiger, fire management, Integrated Development of Wildlife Habitats (IDWH) including the Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA), the lack of priority and policy support to ensure the participation of local communities via the institutions of joint forest management committees slowly made their participation customary. This caused a gradual decline in their effectiveness.
Changed role now
The role of local institutions of gram panchayat or joint forest management committees is now restricted to be a consultative institution instead of being partners in planning and implementation. This indifference and alienation from the participatory planning and implementation of various schemes further affects the harmony between Forest Departments and communities, endangering the protection of forests. This is more relevant while taking up restoration activities including tree planting outside the designated forest areas where motivation and encouragement of stakeholders (especially panchayats and urban local bodies) are crucial.
As committed at Glasgow, India will have to ‘focus much more on climate change and devise strategies and programmes to achieve the net zero target’. Besides reducing the quantum of emissions in a phased manner — itself full of challenges — the approaches for carbon storage and offsetting through natural sinks such as forests need to be given equal priority.
Replicate Telangana model
To achieve net zero targets there is a need to revisit our existing legal and policy mechanisms, incentivise the local communities appropriately and ensure fund flow for restoration interventions, duly providing for the adequate participation of local people in planning and implementation through local institutions. Political priority and appropriate policy interventions (as done recently in Telangana by amending the panchayat and municipal acts for environmental concerns and creating a provision for a Green Fund, or Telangana Haritha Nidhi, for tree planting and related activities) need replication in other States. These should be supported by enabling financial and institutional support mechanisms and negotiations with stakeholders to incentivise local communities to boost efforts to conserve and develop forest resources. Though India did not become a signatory of the Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, the considerations of land tenure and the forest rights of participatory communities with accelerated finances will help aid steps in the race toward net zero. This inclusive approach with political prioritisation will not only help reduce emissions but also help to conserve and increase ‘our forest cover’ to ‘a third of our total area’. It will also protect our once rich and precious biological diversity.

Date:08-01-22
दागी उम्मीदवार
संपादकीय
इससे बेहतर और कुछ नहीं कि निर्वाचन आयोग आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्ती बरतने जा रहा है। इसके तहत उसने राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है कि उन्हें आपराधिक छवि वालों को उम्मीदवार बनाने पर यह बताना होगा कि उनका चयन क्यों किया गया? राजनीतिक दलों को यह जानकारी समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से सार्वजनिक करनी होगी। हालांकि यह व्यवस्था पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में ही लागू हो जाएगी, लेकिन देखना यह है कि राजनीतिक दल इस पर कितनी गंभीरता से अमल करते हैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि चुनाव मैदान में उतरने वाले दागी उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से तमाम जीत हासिल कर विधानसभाओं और लोकसभा में भी पहुंच जा रहे हैं। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाले या फिर उसके लिए खतरा बने लोग ही विधानमंडलों में जाकर कानून बनाने का काम करें? दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। इसके चलते न केवल राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, बल्कि विधानमंडलों में विमर्श का स्तर भी गिरता जा रहा है।
उम्मीद की जाती है कि निर्वाचन आयोग का दबाव रंग लाएगा, लेकिन इसकी भी आशंका है कि राजनीतिक दल आपराधिक छवि वालों को उम्मीदवार बनाने के लिए कोई न कोई आड़ खोज ही लेंगे। आखिर यह एक तथ्य है कि अतीत में राजनीतिक दल दागी छवि वालों को इस बहाने चुनाव मैदान में उतारते रहे हैं कि वे उन्हें सुधरने का मौका देना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग के साथ आम जनता को भी यह देखना होगा कि ऐसी थोथी दलीलों के साथ दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरकर सफल न होने पाएं, क्योंकि आखिर यह जनता ही है, जो जाति, मजहब, क्षेत्र के नाम पर आपराधिक छवि वालों को वोट देने का काम करती है। नि:संदेह जितनी जरूरत निर्वाचन आयोग के स्तर पर यह सुनिश्चित करने की है कि आपराधिक इतिहास वाले चुनाव मैदान में न उतरने पाएं, उतनी ही इसकी भी कि मतदाता भी ऐसे उम्मीदवारों से दूरी बनाए। और भी अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव पर सहमत हों, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि संगीन आरोपों से घिरे उन लोगों को प्रत्याशी बनाना निषेध किया जाए, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका हो। दुर्भाग्य से राजनीतिक दल इस पर यह कहने में लगे हुए हैं कि दोषी सिद्ध न होने तक हर कोई निर्दोष है। अच्छा हो कि वे यह समझें कि यह तर्क राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ा रहा है।

Date:08-01-22
बजट की बुनियादी बातें
टी. एन. नाइनन
जनवरी में सबका ध्यान केंद्रीय बजट पर लगा रहता है। तमाम अन्य चीजों की तरह बजट के मामले में भी गैरजरूरी बातों को किनारे करके जरूरी बातों पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है। बात शुरू करते हैं सरकारी कर्ज से। महामारी से निपटने की कोशिश में घाटा बढ़ा और सरकारी कर्ज में तेजी से इजाफा हुआ। राजस्व को हो रहे नुकसान के दौरान खर्च करना भी अपरिहार्य था और यह अपेक्षाकृत कम ही रहा। इसके बावजूद इसका प्रभाव नजर आ रहा है। केंद्र और राज्यों का सरकारी कर्ज जीडीपी के 90 फीसदी के करीब है। महामारी के पहले यह 70 फीसदी था जबकि इसका वांछित स्तर 60 फीसदी है।
परिणामस्वरूप ब्याज का बोझ बढ़ रहा है। महामारी के पहले यह सरकारी प्राप्तियों के 34.8 फीसदी के स्तर पर था। यह आंकड़ा करीब एक दशक से बदला नहीं था क्योंकि 2011-12 में भी यह 34.6 फीसदी ही था। लेकिन चालू वर्ष के लिए बजट अनुमान के अनुसार ब्याज की हिस्सेदारी बढ़कर 40.9 फीसदी हो गई है। यदि अनुमान 34.8 फीसदी पर बना रहता तो सरकार के पास अपने कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये बचते। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो बिल का आकार और बढ़ेगा। भविष्य के लिए यह बड़ा बोझ होगा और अन्य प्रकार के व्यय को सीमित करेगा।
इसके अलावा बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के हिस्से के रूप में कर राजस्व की हिस्सेदारी अधिक होती है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे तथा रक्षा क्षेत्र का वित्त पोषण किया जा सके। भारत के मामले में जीडीपी के हिस्से के रूप में केंद्रीय सकल कर राजस्व संग्रह लगभग अपरिवर्तित है। 10 वर्ष पहले यह 10.2 फीसदी था और इस वर्ष इसके 9.9 फीसदी रहने का अनुमान है। हालांकि इस आंकड़े में संशोधन हो सकता है क्योंकि कर संग्रह बेहतर है, परंतु कर-जीडीपी अनुपात में दीर्घावधि से चला आ रहा ठहराव दरअसल इसलिए है क्योंकि हमारा देश स्वास्थ्य और शिक्षा तथा रक्षा क्षेत्र पर कम खर्च कर रहा है।
इससे पहली बात तो यह पता चलती है कि बजट भाषण में उल्लिखित वे लंबी-लंबी सूचियां जिनमें सरकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटन में भारी इजाफे की बात कही जाती है वह बस शब्दों की बाजीगरी होती है। यदि जीडीपी के संदर्भ में राजस्व और कुल व्यय में उसी तरह इजाफा नहीं होता है और अगर कुछ कार्यक्रमों को अधिक राशि मिलती है तो यह स्पष्ट है कि औरों को कम राशि मिल रही है।
हाल के वर्षों में राजस्व में ठहराव की एक वजह है वस्तु एवं सेवा कर। इस वर्ष अधिक जीएसटी राजस्व को लेकर आशावादी टीकाकार इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि यह तेजी प्राथमिक तौर पर इसलिए आई है कि आयात में इजाफा हुआ है (दिसंबर तक आयात में 70 फीसदी बढ़ोतरी हुई)। तथ्य यह है कि इस बड़े कर सुधार से राजस्व में अपेक्षित इजाफा नहीं हुआ है और न ही जीडीपी में वृद्धि हुई है। इसकी वजह सब जानते हैं लेकिन सुधार के उपाय धीमे रहे हैं। राजस्व में कमी का एक अन्य कारण कॉर्पोरेशन कर है। वर्तमान मूल्य पर देखें तो जीडीपी गत एक दशक में 160 फीसदी बढ़ा है जबकि कॉर्पोरेशन कर से आने वाला राजस्व केवल 70 फीसदी बढऩे की बात कही गई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो व्यक्तिगत आय कर से हासिल होने वाले राजस्व के एक दशक में 230 फीसदी बढऩे का अनुमान है। यह असंतुलन इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनियां कठिन समय से गुजरी हैं। अच्छी बात है कि हम उस दौर से आगे निकल आए हैं। इसलिए बजट के दिन जब चालू वर्ष के संशोधित कर आंकड़े सामने आएंगे तो ये अनुपात सुधरे हुए दिखेंगे।
इसके बावजूद व्यापक रुझान अपरिवर्तित है: सरकारी राजस्व उस तरह नहीं बढ़ा जिस तरह उसे बढऩा चाहिए था और विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यय राशि में बदलाव एक तय दायरे में ही हुआ है। अगर राजस्व का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज भुगतान में चला जाएगा तो बजट में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य (वृद्धि और रोजगार में इजाफा तथा बढ़ती असमानता को दूर करना) हासिल करने के लिए राजकोषीय उपायों की गुंजाइश और अधिक सीमित रहेगी।
ऐसे में इस स्थिति को दूर करने और राजस्व बढ़ाने के केवल दो तरीके हैं। पहला, तेज आर्थिक वृद्धि। सदी के पहले दशक में ब्याज के भारी बोझ (सरकारी प्राप्तियों के हिस्से के रूप में) से ऐसे ही निपटा गया था। बदकिस्मती से फिलहाल वैश्विक परिस्थितियां अलग हैं। दूसरा है कर नीति और प्रमुख तौर पर जीएसटी सुधारों का दोबारा आकलन करना, कॉर्पोरेट कर की कमियों को दूर करना और यह सवाल करना कि आखिर पूंजीगत लाभ पर लगने वाले कर अर्जित आय पर लगने वाले कर से कम क्यों हैं तथा अस्तित्वहीन संपत्ति पर कर लगाना।
Date:08-01-22
राज्य वह नहीं है जैसा उसे समझा जाता है
आर जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )
आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, चीन की आक्रामकता या जातीय अथवा धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि संस्थानों का नियमित और निरंतर हो रहा क्षरण और / अथवा उनकी निर्बलता है। स्थानीय निकायों से लेकर न्यायपालिका और धार्मिक, जनजातीय, जातीय और सामुदायिक समूहों तक कुछ ही संस्थान (आधुनिक या पारंपरिक) हैं जो साझा उद्देेश्य के लिए काम कर पा रहे हैं। संयुक्तराष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ अथवा विश्व व्यापार संगठन तक कोई संस्थान अपनी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा। कानून व्यवस्था के हाथों जो बचा है उसे राजनेता और गैर सरकारी तत्त्व कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका ने तो अपने कुछ पुलिस बलों की फंडिंग दूसरे विभागों को स्थानांतरित करके एक तरह से उनकी वैधता ही समाप्त कर दी। ब्रेक्सिट, वारसा संधि जैसे अधिराष्ट्रीय निकायों की बात आती है तो विभिन्न देश ऐसा ही चाहते हैं। मौद्रिक नीति से जुड़े संस्थान भी विफल रहे हैं (यही कारण है कि इतनी अधिक आर्थिक उथलपुथल और क्रिप्टो जैसी मुद्राओं में लोगों का भरोसा मजबूत होता दिखता है) और समान जातीयता वाले छोटे देशों के अलावा न्यायपालिका भी हर जगह नाकाम होती दिखती है। कई देशों में कद्दावर नेताओं का उभार कुछ और नहीं बल्कि नागरिकों की यह देखने की दुविधा है कि मजबूत नेता नाकाम होते संस्थानों से बेहतर तो नहीं साबित होगा।
हमें इसकी अपेक्षा करनी चाहिए थी। राज्यों और उनके नेतृत्व वाले संस्थानों को व्यक्तिगत मानवाधिकार के संरक्षण के बदले हिंसा और कानून बनाने का अधिकार सौंप देने की व्यवस्था को नाकाम होना ही था। ऐसा इसलिए कि हमने राज्य शब्द को भौगोलिक संप्रभुता के अनुसार परिभाषित किया है। यह स्वयं इस गलत अवधारणा पर आधारित है कि राष्ट्र एक तरह के लोगों से बनता है जो एक खास भूभाग में रहते हैं। परंतु ऐसा कभी नहीं रहा क्योंकि लोग तो हर जगह जाते हैं और वहां के जनांकीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। आज कई यूरोपीय राज्यों को यह अहसास है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पुलिस भी नहीं जा सकती। जर्मनी की पिछली चांसलर एंगेला मर्केल ने भी यह बात स्वीकार की थी। ब्रिटेन में ग्रूमिंग स्कैंडल में 11 से 16 वर्ष की उम्र की बच्चियों के खिलाफ यौन अपराध हो सके क्योंकि पुलिस से कहा गया था कि पाकिस्तानी गैंगों के खिलाफ कार्रवाई करना राजनीतिक दृष्टि से अनुचित होगा। ब्रिटिश पुलिस अपनी ही महिलाओं का बचाव करने में नाकाम रही और अपनी वैधता गंवा बैठी।
दरअसल कई तरह के राज्य मौजूद हैं और राज्य का अर्थ केवल सरकार, विधायिका, न्यायपालिका अथवा कानून प्रवर्तन नहीं है। इसमें सभी संस्थान शामिल होते हैं जो व्यक्तियों पर अधिकार दर्शाते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम उनक प्राधिकार को वैध मानते हैं या अवैध। इस परिभाषा के मुताबिक परिवार एक सूक्ष्म राज्य है क्योंकि यह परिवार की परिभाषा में आने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। जनजातियां और समुदाय भी एक राज्य बनाते हैं क्योंकि उनका भी अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण होता है। कॉर्पोरेट निकाय भी अद्र्ध राज्य होते हैं क्योंकि वे अपने कर्मचारियों, वेंडरों और वितरकों पर व्यवहार थोप सकते हैं, भले ही उनका प्रभाव विशुद्ध रूप से आर्थिक हो और कार्यस्थल तक सीमित हो। गूगल, फेसबुक (अब मेटा), ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट आदि सभी साइबर राज्य हैं और अक्सर वे अपने ‘नागरिकों के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से ज्यादा जानते हैं। अपराध माफिया भी एक राज्य है। उसके पास भी समय-समय पर कुछ लोगों से अपन बात मनवाने का अधिकार होता है। पुलिस की बात करें तो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी अपराधी समूहों से संपर्क में रहते हैं। उदारवादी परियोजना को कभी न कभी नाकाम होना ही था, उसने हर दूसरे संस्थान की वैधता नष्ट करने का प्रयास किया क्योंकि उनमें सुधार नहीं किए गए या उन्हें दमन के उपकरण माना गया।
यह मानना महत्त्वपूर्ण है कि पारंपरिक संस्थान एक स्तर तक दमनकारी थे, लेकिन राज्य शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश राज्य की शक्तिको ही अवैध बनाती है। यदि केवल राज्य और निजी व्यक्ति ही शेष रह गए तो एक स्तर के बाद राज्य इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह व्यक्तियों के अधिकारों को ही क्षति पहुंचाएगा। इसे गैर राज्य शक्तियों द्वारा राज्यों को धमकाने और राज्यों द्वारा कथित तौर पर नागरिकों की रक्षा के नाम पर निजता भंग करने के और अधिकारों की मांग करने और कानून बनाने में देखा जा सकता है।
सवाल यह है कि क्या हमने खुद के लिए जो गड्ढा खोदा है हम उससे बाहर निकल सकते हैं? जवाब कई बातों पर निर्भर करता है और खासतौर उदार कुलीन वर्ग की गलतियां मानने और सुधारने की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। दरअसल उन्हें लगता है कि ज्ञान और बुद्धिमता पर उनका एकाधिकार है। वे चाहते हैं कि हम राज्य और व्यक्तिगत अधिकारों की उनकी परिभाषा स्वीकार करें, वाक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के मामले में भी वे ऐसा ही चाहते हैं। आम समझ कहती है कि बिना नियंत्रण के वाक स्वतंत्रता से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है (हरिद्वार में साधुओं की बैठक इसकी बानगी है)। धर्म की पूर्ण आजादी का अर्थ है दूसरों के धर्मांतरण का असीमित अधिकार। यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है कि अपने विस्तार की इच्छा रखने वाला कोई भी धर्म दूसरों का दमन करके ही ऐसा कर सकता है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ेगी। देश और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। इससे निपटने का तरीका यही है कि पारंपरिक संस्थानों की वैधानिकता लौटाई जाए और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को नियमों और आंतरिक नियमन को लेकर कुछ आजादी प्रदान की जाए। प्रयोग के स्तर पर बेहतर होगा कि राज्य पारंपरिक संस्थानों का इस्तेमाल उनके संचालन का काम करे जो उसके प्रति निष्ठा रखते हों, न कि यह दर्शाते हुए कि उनकी कोई वैधता नहीं है। ऐसे पारंपरिक संस्थानों की सामाजिक पूंजी होती है। धार्मिक संस्थानों से लेकर खाप पंचायतों तक इसका इस्तेमाल उन्हें अधिक जवाबदेह और आत्मनियमन वाला बनाना चाहिए। राज्य सरकार तब अपराधियों और आतंकवादियों को आसानी से पकड़ सकेगी जब उन समुदायों से जिनसे वे आते हैं, उन्हें पता हो कि अगर वे अपने बीच के पथभ्रष्ट लोगों को न्याय की दहलीज पर नहीं ले जाएंगे तो वे अधिकार गंवा बैठेंगे।
लब्बोलुआब यह कि पारंपरिक संस्थानों को सीमित वैधता प्रदान करना भी समाजों और राष्ट्रों को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। राज्य लोगों के जीवन पर एकाधिकार नहीं रख सकते।

Date:08-01-22
खर्च की सीमा
संपादकीय
वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग का चुनाव खर्च बढ़ाने का फैसला उचित कहा जा सकता है। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च का अनुमान भी लगाता है। उसी के अनुसार खर्च सीमा तय करता है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा अट्ठाईस लाख रुपए से बढ़ा कर चालीस लाख रुपए कर दी है। इसी तरह लोकसभा के लिए पंचानबे लाख रुपए तय किया गया है।
नियम के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी तय सीमा से अधिक पैसा चुनाव पर खर्च नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्याशियों को बाकायदा अपने खर्च का प्रमाण भी जमा कराना पड़ता है। उसके जमा कराए प्रमाण और खर्च संबंधी दावों की जांच भी की जाती है। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च कर रहा है, तो उसे नोटिस भी जारी करता है। मगर हकीकत यह भी है कि अब तक इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया गया है। फिर यह भी छिपी बात नहीं कि गिने-चुने ऐसे प्रत्याशी होंगे, जो निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा में धन खर्च करते हैं। ये वही लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते। वरना आजकल ग्राम पंचायत जैसे मामूली चुनावों में भी कई प्रत्याशी चालीस लाख से अधिक रुपए खर्च कर देते हैं।
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव धीरे-धीरे धनबल और बाहुबल के आधार पर लड़े और जीते जाने लगे हैं। इस तरह इन चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए महंगे उपहार देने की परंपरा धड़ल्ले से चल निकली है। नगदी बांटने का भी खूब चलन है। हर चुनाव में निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर नगदी, शराब, महंगे उपहार आदि की जब्ती करता है। इसके अलावा प्रचार सामग्री के रूप में आकर्षक पोस्टर, बड़े-बड़े बैनर, होर्डिंग, आसमान छूते कट-आउट और संचार माध्यमों में महंगे विज्ञापन पर अकूत पैसा खर्च किया जाता है। अब तो अपने पक्ष में खबरें छापने या बनी-बनाई खबरें छापने के लिए पैसे देने का चलन भी सुनने को मिलता रहता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तय सीमा के बावजूद प्रत्याशी चुनाव में कितना पैसा खर्च करता होगा, इसका ठीक-ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल बना रहता है। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए तो खर्च सीमा तय कर रखी है, पर पार्टियों के लिए कोई सीमा तय नहीं की है। इसकी आड़ लेकर प्रत्याशी अपना बहुत सारा खर्च पार्टी के हिस्से में दिखा देते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि जो राजनीतिक दल चंदे के मामले में जितना संपन्न है, उसका प्रत्याशी अपने चुनाव में उतना ही अधिक पैसे खर्च करता है।
चुनावों में गैरकानूनी ढंग से जमा किए गए पैसे को जायज बनाने का धंधा भी बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए तमाम विशेषज्ञ लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी और पार्टियों के चुनाव खर्च पर अंकुश लगाने का कोई व्यावहारिक उपाय किया जाना चाहिए। मगर अब तक इस दिशा में कोई व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत किसी ने नहीं समझी है। दरअसल, राजनीतिक दल खुद चंदे के खेल में इस कदर होड़ में लगे रहते हैं कि वे काले धन पर रोक लगाने के लिए इस पहलू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तय सीमा का बहुत मतलब नहीं रह जाता।
Date:08-01-22
जनसंख्या और विकास
विजय प्रकाश श्रीवास्तव
चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के एक वर्ग के अनुसार देश की तमाम समस्याओं मसलन बेरोजगारी, गरीबी आदि के मूल में हमारी विशालकाय आबादी ही है। हमारे शासकों में भी, चाहे वे किसी भी दल से रहे हों, आबादी को विकास में रोड़ा मान कर अपना पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति देखने को मिलती रही है। देश में पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी। अब यह जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर हुआ करती है। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ अन्य सर्वेक्षण भी होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है- राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो 1992-93 में पहली बार किया गया था। 2019-21 के दौरान किए गए ऐसे पांचवें सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल में जारी की गई है। इस सर्वेक्षण में कई नई बातें सामने आई हैं।
सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश की जनसंख्या में दशक भर पहले तक निरंतर वृद्धि की जो प्रवृति दिखती थी, उस पर विराम लग गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रजनन दर 2.1 की आकलित प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह वह स्तर है जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय बस इसमें कमी की भरपाई करती है। प्रति स्त्री औसत संतान जन्म दर 2015-16 के 2.2 से घट कर 2.0 पर आ टिकी है। भले ही यह गिरावट सिर्फ 0.2 की हो, पर पूरे देश के लिए यह आबादी में वृद्धि की बजाय बड़ी गिरावट का संकेत देती है। यदि जन्म दर यही बनी रही तो देश की आबादी घटती हुई नजर आएगी।
आपातकाल में परिवार नियोजन के ‘जबरन’ प्रयासों को छोड़ दिया जाए तो भारत की जनसंख्या नीति आमतौर पर उदार रही है। इस मामले में चीन जैसी सख्ती लागू करने की बात कभी नहीं सोची गई। जनता के लिए जनसंख्या नियंत्रण के जो भी सरकारी उपाय लागू हैं, वे प्राय: सुझावात्मक हैं न कि बाध्यकारी। कुछेक अपवादों को छोड़ कर जैसे कि कतिपय राज्यों में दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है।
दुनिया में संसाधन सीमित हैं। ऐसे में जब संसाधन कम हों और लोग ज्यादा हों, तो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम होगी। अगर लोग कम होंगे तो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा होगी। इस कथन की पुष्टि के लिए जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जैसे विकसित देशों का उदाहरण दिया जाता है। पर इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। कहीं न कहीं विकसित देश संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जनसंख्या को अधिक सक्षम तथा योग्य बनाने में उच्चतर निवेश भी करते हैं। यदि हम अपने देश की जनसंख्या को देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मानते रहे हैं तो इस दृष्टिकोण को बदलने का समय आ गया है।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास के प्रारंभिक चरणों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची होती है। आय का स्तर बढ़ने के साथ साक्षरता में भी वृद्धि होती है और जन्म दर में कमी आने लगती है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो परिणाम आए हैं, उन्हें इसके साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। जनसंख्या यदि समस्या बनी रहती है तो इसकी वजह यह है कि इसमें निहित संभावनाओं का लाभ नहीं उठाया जाता।
भारत के मामले में तो यह पूरी तरह सही है। देश में ऐसे करोड़ों युवा हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। अगर ये अर्थपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगे होते तो न केवल उनकी स्थिति बेहतर होती, बल्कि देश भी बेहतर स्थिति में होता, चाहे इसे सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के संदर्भ में देखा जाए या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में।
कहा जाता है कि गरीबी तथा जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, पर नवजात मृत्यु दर भी गरीब वर्ग में ही अधिक पाई जाती है। इसलिए बच्चे जीवित रहें, इस आस में उनके यहां संतानोत्पत्ति की दर अधिक होती है। साथ ही निर्धन परिवारों का दृष्टिकोण यह होता है कि हर बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही काम में लग कर कमाई करने लगेगा और इससे परिवार की आय बढ़ेगी। यदि गरीबों की आय का स्तर ऊंचा उठे जिससे वे सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकें तो इस वर्ग में जन्मदर में कमी आ सकती है।
विकास का चक्र जनसंख्या के स्वरूप और आकार से सीधे संबद्ध है। शिक्षित-प्रशिक्षित कौशलयुक्त जनसंख्या जब पूरी तरह उत्पादक कार्यों में नियोजित होती है तो उनका और उनके परिवार का आय स्तर उठता है, आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि होती है जिसके साथ मांग का स्तर भी बढ़ता है। इस प्रकार रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है और यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है।
सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को पूरी तरह तो नहीं मिटाया जा सकता, पर उनका न्यूनीकरण करने पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा एक मामला महिलाओं के लिए अवसरों को लेकर है। उदाहरण के तौर पर, भारत में सेवा उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। रोजगार के ज्यादातर नए अवसर इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। आनुपातिक रूप से सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, चाहे यह सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो अथवा काल सेंटर उद्योग। पर हमारे देश में एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र भी है और इसमें महिलाएं अत्यंत कम संख्या में नियोजित हैं। चाहे वाहन निर्माण का कारखाना हो अथवा उपभोक्ता वस्तुओं जैसे वाशिंग मशीन और फ्रिज आदि बनाने का, आपको गिनी-चुनी महिलाएं ही कार्य करती हुई दिखाई देंगी। रूस आदि देशों में महिलाएं ट्रक चलाने जैसे कार्य कई दशकों से कर रही हैं, पर अपने देश में हम उन्हें शारीरिक क्षमता वाले कार्यों से दूर रखते रहे हैं। हाल में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे युवतियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसे एक नई शुरुआत मान कर विनिर्माण उद्योग में भी महिलाओं के नियोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
यदि आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है तो रोजगार में भी उनका प्रतिनिधित्व इसी अनुपात में होना चाहिए। पर इसमें कई अड़चनें हैं। एक तो शिक्षा के अवसरों को लेकर असमानताएं हैं, दूसरे कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार रही है जिसमें यह मान लिया गया था कि महिलाओं की हद चूल्हे-चौके तक है। पर अब यह सोच पीछे छूट रही है। श्रम बल तथा रोजगार में महिलाओं को और बड़ी संख्या में लाने की जरूरत है। यह लैंगिक समानता तथा समावेशी समाज के लिए तो आवश्यक है ही ,अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत करने के लिए भी अपरिहार्य है। सोचने की बात है कि पश्चिमी देशों का विकसित देशों की श्रेणी में आना महिलाओं की व्यापक भागीदारी के बिना क्या संभव हो पाता? अब जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है और उनमें अपने हितों तथा स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसे हमारे देश के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें सबसे अधिक जोर शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने, बुनियादी सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, कौशल विकास के दायरे में अधिकाधिक लोगों को लाने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर होना चाहिए। भारत को यदि विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो अवसर हमारे सामने है।

Date:08-01-22
चुनाव आयोग की कवायद
संपादकीय
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कोरोना विषाणु के नये स्वरूप ओमीक्रोन के खतरों के बीच होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग ने पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना विषाणु के संक्रमण‚फैलने की तीव्रता दर‚कथाम के उपायों और टीकाकरण को लेकर पारस्परिक विमर्श हुआ। इसके बाद चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी विचार–विमर्श किया। अब देखना है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का क्या परिणाम सामने आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग उन सभी उपायों पर विचार कर रहा है जिससे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोरोना के प्रसार को रोका जाए। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कांग्रेस के बाद भाजपा और सपा ने भी उत्तर प्रदेश में अपने–अपने चुनावी रैलियों को रद्द करने का फैसला किया है। चुनावी रैलियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की आलोचना हो रही थी। पिछले एक सप्ताह से देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक लाख को पार कर गई। महामारी विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो तीसरी लहर की घोषणा कर दी है‚ लेकिन यह विश्व मानवता के लिए सौभाग्य की बात है कि कोरोना विषाणु का नया स्वरूप ओमीक्रोन डे़ल्टा के मुकाबले कम घातक है। यही कारण है कि ड़ब्ल्यूएचओ इसे सुनामी की संज्ञा दे रहा है। अमेरिका में पिछले दिन एक दिन में 10 लाख से ज्यादा नये मामले आए थे। यूरोपीय देशों में भी रोजाना एक से दो लाख नये मामले आ रहे हैं‚ लेकिन संतोष की बात यह है कि कोरोना विषाणु के प्रकटीकरण के पिछले दो वर्षों के दौरान दुनिया के लोग इस वायरस से परिचित हो गए हैं। और हमारे देश में भी कोरोना के विरुद्ध दर्जनों वैक्सीन उपलब्ध हैं तथा अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी के संबंध में एक व्यापक आधारभूत ढांचा मौजूद है। इसके बावजूद आयोग विभिन्न दलों के साथ बैठक करे और कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए एक साझा कार्यक्रम बनाए। ऐसा इसलिए कि देश में कहीं–न–कहीं कोई–न–कोई चुनाव होते रहते हैं और कोरोना भी अभी हाल–फिलहाल जाने वाला नहीं है।
Date:08-01-22
भारत के लिए स्थायी सुरक्षा चुनौती बन गया है चीन
सी उदय भास्कर, ( निदेशक, सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज )
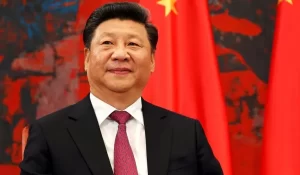 इस साल भारत के सामने जो तीन स्थाई सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं, वे ‘सी’ अक्षर वाली हैं- ओमीक्रोन वेरिएंट के साथ कोविड-19, क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) और चीन। मुमकिन है कि ये अलग-अलग रूपों में सामने आएं, मगर तीनों चुनौतियां राष्ट्रीय नेतृत्व के नीति-कौशल की परीक्षा ले सकती हैं। कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट पारिस्थितिकीय असंतुलन के बढ़ने से पैदा हुए जटिल मसले हैं और वैश्विक स्तर पर इनका हल भी खोजा जा रहा है। पर चीन हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2020 के मध्य में गलवान हिंसा और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कायम गतिरोध को देखते हुए हमें हालिया घटनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। जैसे, नए साल के मौके पर एक तरफ तो भारतीय व चीनी सैनिकों के एक-दूसरे को मिठाई बांटने वाले दृश्य दिखे, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वीडियो क्लिप साया हुई, जिसमें उसके जवान गलवान घाटी में अपना झंडा फहराते दिख रहे थे। ऐसा लगता है कि बीजिंग ने विवादित क्षेत्र पर खुद को मजबूत बनाना अपनी प्राथमिकता बना ली है। पैंगोंग झील पर पीएलए द्वारा पुल-निर्माण भी इसी मंशा का सुबूत है।
इस साल भारत के सामने जो तीन स्थाई सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं, वे ‘सी’ अक्षर वाली हैं- ओमीक्रोन वेरिएंट के साथ कोविड-19, क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) और चीन। मुमकिन है कि ये अलग-अलग रूपों में सामने आएं, मगर तीनों चुनौतियां राष्ट्रीय नेतृत्व के नीति-कौशल की परीक्षा ले सकती हैं। कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट पारिस्थितिकीय असंतुलन के बढ़ने से पैदा हुए जटिल मसले हैं और वैश्विक स्तर पर इनका हल भी खोजा जा रहा है। पर चीन हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2020 के मध्य में गलवान हिंसा और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कायम गतिरोध को देखते हुए हमें हालिया घटनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। जैसे, नए साल के मौके पर एक तरफ तो भारतीय व चीनी सैनिकों के एक-दूसरे को मिठाई बांटने वाले दृश्य दिखे, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वीडियो क्लिप साया हुई, जिसमें उसके जवान गलवान घाटी में अपना झंडा फहराते दिख रहे थे। ऐसा लगता है कि बीजिंग ने विवादित क्षेत्र पर खुद को मजबूत बनाना अपनी प्राथमिकता बना ली है। पैंगोंग झील पर पीएलए द्वारा पुल-निर्माण भी इसी मंशा का सुबूत है।
दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय की इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दें, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली ने कमोबेश मौन अपनाया है। रक्षा मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा में भी उसका यही रवैया दिखता है। इसमें आत्मनिर्भरता और कई अन्य उपलब्धियों (नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत और एकीकृत सैन्य कमांड की ओर बढ़ना आदि) को बताने वाली एक लंबी और व्यापक समीक्षा में नियंत्रण रेखा और चीन का संदर्भ कमतर है। इसमें यह जिक्र तक नहीं है कि उसने लद्दाख क्षेत्र में करीब 1,000 वर्गमील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। चीन की हठधर्मिता के सामने क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना निस्संदेह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यही वह जगह है, जहां सच हमें बेचैन करता है। दरअसल, चीन और भारत के बीच सर्वसमावेशी राष्ट्रीय ताकत का अंतर बीजिंग के पक्ष में बढ़ गया है और यह तस्वीर हाल-फिलहाल में शायद ही बदल सकेगी। एलएसी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सैन्य क्षमता को सामरिक रूप से बेशक बढ़ाया गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे पुनर्गठन कहा जाएगा, क्योंकि यहां इन्वेंट्री या गोलाबारी क्षमता में शायद ही उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
स्वाभाविक है कि यह बजट आवंटन का मामला है और कोविड-19 के कारण के कई क्षेत्रों में खर्च घटाए गए हैं। हमारा रक्षा बजट अब भी कम है। यह हकीकत अगले दो वर्षों में शायद ही बदल सकेगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्रभावी अधिकार जमाने रखने की दिशा में भारत को नीतिगत मोर्चे पर दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बत के मुद्दे पर भारत स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारतीय सांसदों को दी गई बेशर्म सलाह, अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामों में एकतरफा बदलाव और भारतीय जमीन पर व हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल इस साल भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्ते का भविष्य बताने को काफी हैं।
यह सच भी हमारी नीतिगत दुविधा बढ़ा रहा है कि एलएसी तनाव के बावजूद चीन के साथ हमारा कारोबारी रिश्ता मजबूत हो रहा है। पिछले 11 माह में कुल व्यापार 114.46 अरब डॉलर का रहा, जो रिकॉर्ड स्तर है। इसमें हमने चीन से 87.9 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात 26.36 अरब डॉलर का। प्रमुख कारोबारी गठबंधनों से बाहर रहने का विकल्प चुनने के बाद भी चीन को कमतर करने की योजनाएं सीमित रह बची हैं।
यह समझना होगा कि सैन्य शक्ति प्रदर्शित करते हुए सख्त राजनीतिक संबंध कूटनीति को अधिक प्रभावी बनाता है, इसलिए भारत को चीन के साथ रिश्ते में अपनी सैन्य क्षमताओं को अधिक स्पष्ट तरीके से जाहिर करना चाहिए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में संसद में पेश की गई सैन्य क्षमता का आकलन करने वाली खंडूरी रिपोर्ट पर फिर से गौर करना, और इसमें की गई सिफारिशों पर अमल करना आवश्यक है। मगर अपने यहां तो कोई आधिकारिक भारतीय ‘स्रोत’ पैंगोंग झील को चीन का ‘हिस्सा’ तक बता देता है।
WhatsAppFacebookTwitterPinterestEmailShare

